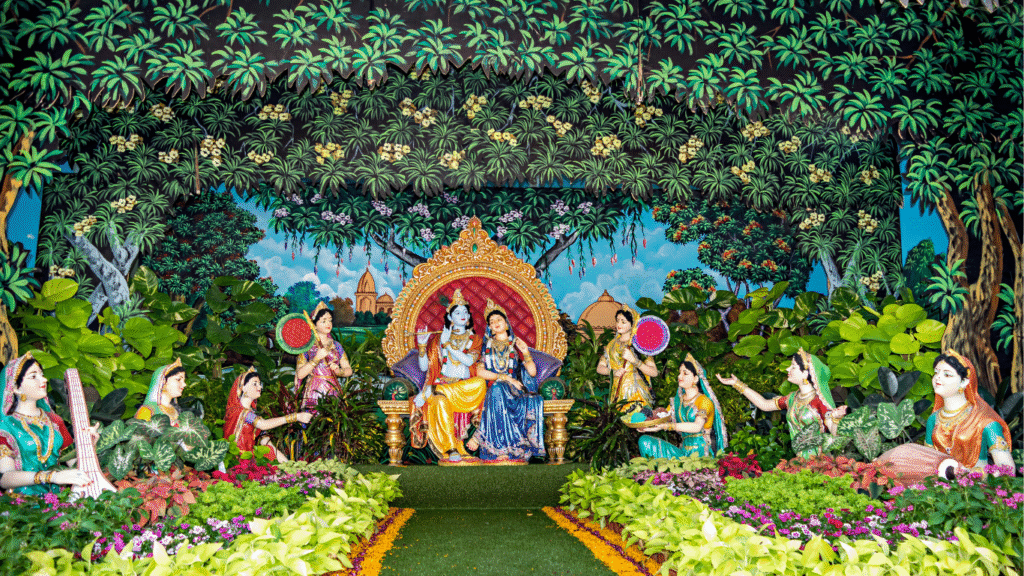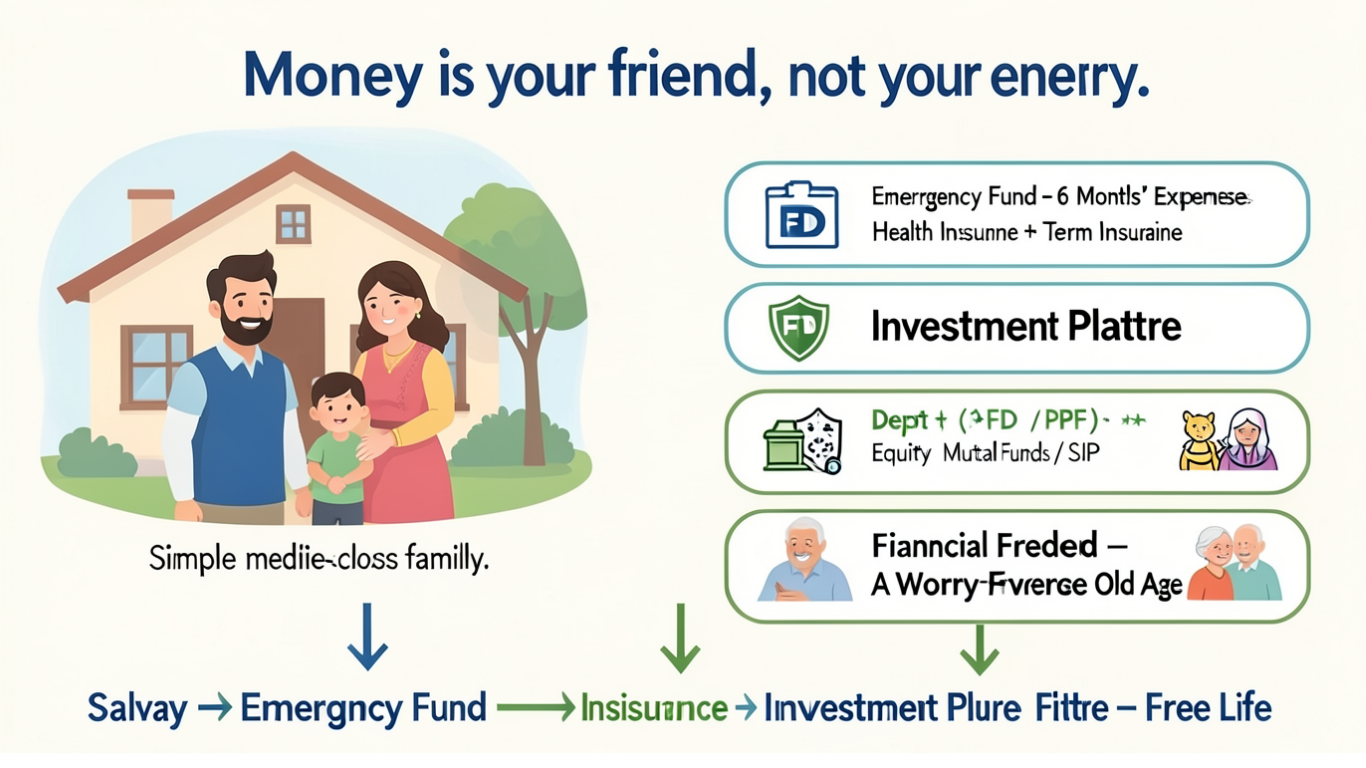यह वीडियो “How ‘Civic Sense’ Has Become the NEW Tool to Shame India?” एक समकालीन और समाजशास्त्रीय विषय पर केंद्रित है, जिसमें बताया गया है कि भारत में ‘सिविक सेंस’ (Civic Sense) का मुद्दा किस तरह सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भारत की छवि को कमजोर करने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। इस लेख में हम वीडियो के प्रमुख तर्क, संदर्भ, सामाजिक निष्कर्ष और सुधार के उपायों को विस्तारपूर्वक प्रस्तुत किया.
प्रस्तावना
आज जब भारत आजादी के 78 वर्ष बाद भी अपनी सभ्यता, संस्कृति और विविधता में गर्व महसूस करता है, वहीं दूसरी ओर मानसिक गुलामी और पश्चिमी वैलिडेशन का जाल आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा घेरे हुए है। वीडियो की शुरुआत इसी मानसिक गुलामी की अवधारणा से होती है जिसमें दर्शाया गया है कि देश ने अपनी ज़मीन तो वापस ले ली, लेकिन सोचने का तरीका अब भी उपनिवेशवादी प्रभाव में है।
सिविक सेंस: मुद्दा, परिप्रेक्ष्य और मनोवैज्ञानिक प्रभाव
भारत में ‘सिविक सेंस’ या नागरिक बर्ताव का मुद्दा कोई नया नहीं है। वास्तव में, देश में आज भी सार्वजनिक सफाई, ट्रैफिक नियम, और सामूहिक अनुशासन जैसी समस्याएं बड़े स्तर पर मौजूद हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स ‘सिविक सेंस’ के नाम पर शेमिंग और निगेटिविटी फैलाने का टूल बन गए हैं। जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब यह एक कैंपेन के रूप में ‘इंडिया हेट’ का रूप लेने लगता है।
मनोवैज्ञानिक प्रभाव
वीडियो यह स्पष्ट करता है कि यह सब केवल यूट्यूब व्यूज और फॉलोवर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक कारण से जुड़ा हुआ है—’इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स’ (हीनभावना)। उपनिवेशकाल के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को यह विश्वास दिलवाया कि वे पिछड़े, गंदे और अनसिविलाइज्ड हैं, और समय के साथ यह सोच शिक्षा प्रणाली और सामाजिक व्यवहार में रच-बस गई।
पनपी हुई यह भावना आज सोशल मीडिया द्वारा कई गुना बढ़ गई है। आज विदेशी ब्लॉगर या व्लॉगर भारत की गलियों में घूमकर कमेंट करता है कि ‘इंडियंस स्मेल बैड’, तो हमारे ही देश के लोग उस बात को सत्य मानते हैं, बजाय उसके विरोध में खड़े होने के।
वायरल क्लिप्स और वास्तविकता
वीडियो में एक वायरल किस्से की चर्चा की गई है, जिसमें एक विदेशी लड़की भारतीय गार्ड को कचरा देती है, और गार्ड कचरा दूसरे प्लॉट में फेंक देता है। इस वीडियो को लेकर बड़ी चर्चा होती है कि भारत में लोग सफाई के प्रति लापरवाह हैं। परन्तु जब इस घटना की तहकीकात की गई, तो पता चला कि यह वीडियो एक प्री-प्लांड सेट-अप था, जिसमें विदेशी लड़की ने खुद गार्ड को निर्देश दिया था कि वह कूड़ा दूसरी जगह फेंक दे ताकि एक नेगेटिव कंटेंट बन सके।
यह उदाहरण इस बात की ओर इंगित करता है कि हर वायरल क्लिप की सत्यता को परखे बिना उसे भारत की छवि से जोड़ना गलत है। अधिकतर ऐसी क्लिप्स प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती हैं, जिनका उद्देश्य देश को बदनाम करना है।
भारतीय क्रिएटर और वेस्टर्न वेलिडेशन
एक बड़ी समस्या यह है कि जब कोई विदेशी या वेस्ट की ओर से भारत को लेकर कोई निगेटिव नैरेटिव तैयार किया जाता है, तो भारतीय क्रिएटर्स और सोशल मीडिया यूजर्स उसे आंख मूँदकर आगे बढ़ा देते हैं। पश्चिम की ओर से भारत के लिए कोई भी टिपण्णी हमारे लिए सत्य की तरह है, फिर चाहे वह सत्य हो या झूठ।
इस प्रवृत्ति का परिणाम यह होता है कि जब विदेशी मीडिया या पत्रकार भारत के खिलाफ कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वे उन्हीं भारतीयों द्वारा बनाई गई सोशल मीडिया पोस्ट्स को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा असर न केवल देश की छवि, बल्कि उसकी डिप्लोमेसी, व्यापार, पर्यटन, निवेश आदि सभी क्षेत्रों पर पड़ता है।
बायस्ड नैरेटिव: या तो ‘इंडिया शाइनिंग’, या ‘इंडिया डिसगस्टिंग’
आजकल भारत को या तो पूरी तरह चमकता हुआ, तकनीकी रूप से समृद्ध, शक्तिशाली देश के रूप में दिखाया जाता है या फिर एक बेहद गरीब, गंदगी से भरा, लाचार देश के रूप में। मिडिल ग्राउंड यानी यथार्थवादी चित्रण बेहद कम मिलते हैं।youtube
पश्चिमी देशों की तुलना करते हुए वीडियो बताता है कि हर देश में अपनी समस्याएँ हैं—अमेरिका में गन वायलेंस, नशाखोरी, रेप की घटनाएँ, यूरोप में क्राइम, शरणार्थी संकट आदि। लेकिन वहाँ के नागरिक इन समस्याओं को ग्लोबल शेमिंग में नहीं बदलते, वे उन्हें सुधारने पर ध्यान देते हैं।
रेसिज़्म और क्रिटिसिज्म के बीच फर्क
वीडियो भविष्य के लिए यह चेतावनी देता है कि सही आलोचना और रेसिज़्म के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। अगर कोई कहता है कि भारतीय लोगों से बदबू आती है, तो यह आलोचना नहीं बल्कि नस्लभेदी मानसिकता (रेसिज़्म) दर्शाता है । देश में नागरिक जागरूकता बढ़ानी चाहिए, समस्याओं को उजागर भी करना चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य समाधान ढूँढना होना चाहिए, न कि देश को शर्मिंदा या बदनाम करना।
समाधान और आगे की राह
वीडियो समाधान की दिशा में कई महत्वपूर्ण बातें बताता है—
- हर देश अपनी समस्याओं को इंटरनली एड्रेस करता है, उसे ग्लोबल शेमिंग में नहीं बदलता।youtube
- सोशल मीडिया पर वायरल हो रही क्लिप्स की सत्यता को वेरीफाई करें और तब ही उसे आगे बढ़ाएँ।
- अपनी उपलब्धियों को भी उतनी ही मुखरता से फैलाएँ जितना अपनी कमियों को।youtube
- सिविक सेंस की समस्या को आपसी जागरूकता, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्ट्रिक्ट लॉज के माध्यम से सुधारा जा सकता है, जैसे सिंगापुर ने अपने देश को 10 वर्षों में एशिया का सबसे साफ देश बना दिया।youtube
- वैश्विक वैलिडेशन और ‘रिस्पेक्ट’ की भीख माँगना छोड़कर, खुद को आत्म-मूल्य देना और राष्ट्र की गरिमा का संवर्धन करना जरूरी है।
वीडियो में उल्लेखित एक और महत्वपूर्ण आँकड़ा है—एक दशक पहले भारत में केवल 38% लोगों के पास टॉयलेट था, लेकिन आज देश रिकॉर्ड समय में ओपन डिफेकशन फ्री घोषित हो चुका है। इससे स्पष्ट होता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है तो माइंडसेट भी बदलता है।
भारतीय समाज और सोशल मीडिया: दोधारी तलवार
सोशल मीडिया और इंटरनेट बहुत ही शक्तिशाली टूल हैं, जिनका लाभ सही दिशा में किया जा सकता है, तो वहीं थोड़ा सा दुरुपयोग पूरे देश की छवि को नकारात्मक बना सकता है। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, हमें हर जानकारी पर विश्वास करने या गैर-जिम्मेदार तरीके से उसे फैलाने से पहले उसकी सत्यता को परखना चाहिए।
इसके अलावा, डिजिटल नागरिकता का मतलब केवल इंटरनेट चलाना नहीं बल्कि डिजिटल नैतिकता को भी समझना है।
निष्कर्ष
‘सिविक सेंस’ पर चर्चा और उसका प्रचार-प्रसार समाज में कहीं अधिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। परंतु, इसका उपयोग किसी राष्ट्र या सम्पूर्ण समुदाय को शर्मिंदा करने का हथियार बन जाए तो यह गलत है।
आज, समय की माँग है कि भारत के नागरिक ‘सेल्फ रिस्पेक्ट’ और ‘सेल्फ क्रिटिसिज्म’ के बीच अंतर को समझें। जब राष्ट्र की आलोचना हो तो समाधान केंद्रित सोच के साथ उसे ठीक करें, और अगर उपलब्धियाँ हों तो उन्हें भी गर्व से वैश्विक मंच पर प्रसारित करें।
सिविक सेंस और सार्वजनिक अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए हमें पश्चिमी वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं। असली बदलाव अपने आत्म-मूल्यांकन, जागरूकता, उचित इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रभावशाली नीतियों के माध्यम से ही संभव है। हम तभी सही नागरिक बन सकते हैं जब समस्या को पहचानकर समाधान की ओर बढ़ें, न कि खुद को या अपने देश को शर्मिंदा करने में समय गंवाएँ।
इस गहन विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में सिविक सेंस की बहस कई सामाजिक, ऐतिहासिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जुड़ी हुई है। अगर जागरूकता और आलोचना से समाज में सुधार लाना है, तो हमें उस लाइन को समझना होगा, जहाँ सुधार की चाहत देशद्रोह या आत्म-हीनता में न बदल जाए। तभी एक स्वस्थ, जागरूक व गर्वीला भारत संभव हो पाएगा, जिसे किसी बाहरी वेलिडेशन की आवश्यकता नहीं होगी।