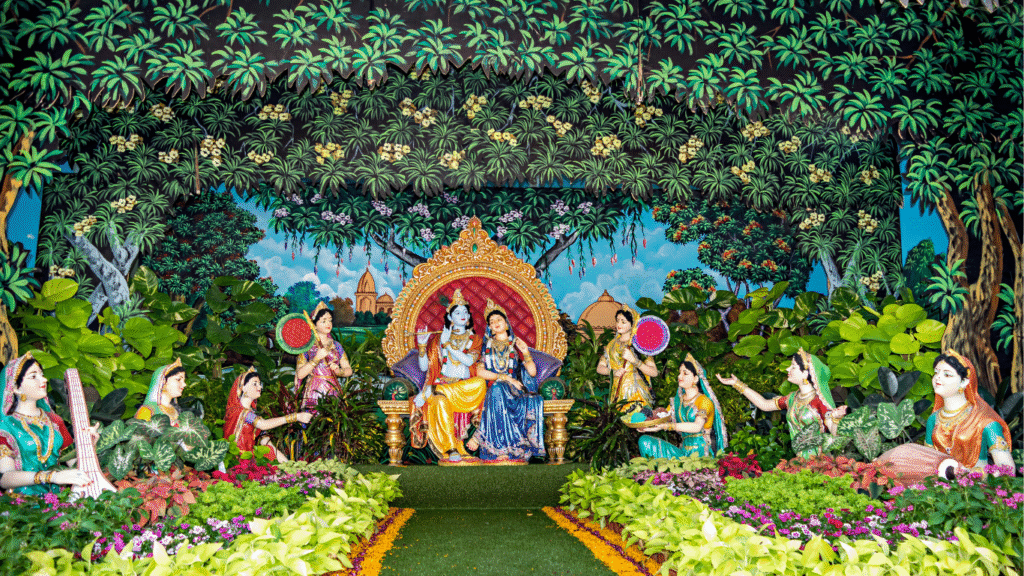राजीव प्रताप – उत्तरकाशी का वह पत्रकार, जिसने स्थानीय अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार का सच उजागर करने का साहस दिखाया और फिर उसकी लाश नदी के बैराज में बरामद हुई। यह घटना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है; यह एक पूरे सिस्टम की पोल खोलती है, जहां सच बोलने का परिणाम इतना भयावह हो सकता है कि उसे मौत कहा जाए। इस लेख में हम राजीव प्रताप के मामले को विस्तार से समझेंगे, पत्रकारों के समक्ष खड़े खतरों का विश्लेषण करेंगे, और सवाल करेंगे कि क्या भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना अब भारत में गुनाह बन गया है। इस पूरी घटना की जड़ में छुपी सच्चाई, राजनीतिक तंत्र की अक्षमता, और पत्रकारों के अधिकारों एवं सुरक्षा की उपेक्षा को आप तक पहुँचाने का प्रयास है।
घटनाक्रम: सच उजागर करने की कीमत
राजीव प्रताप उत्तरकाशी जिले के पत्रकार थे, जिन्होंने हाल ही में अपने निजी यूट्यूब चैनल – ‘दिल्ली उत्तराखंड’ पर स्थानीय जिला अस्पताल की दयनीय हालत और वहां के व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार पर रिपोर्टिंग की। उन्होंने अपनी अंतिम रिपोर्ट में दिखाया कि ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारी अस्पताल परिसर में शराब पीते हैं, गंदगी फैली रहती है, इलाज की व्यवस्था न के बराबर है, और प्रणाली पूरी तरह से भ्रष्ट है। 12 दिन पहले उन्होंने यह वीडियो रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। उनके परिवार ने बताया कि कई अंजान नंबरों से कॉल आ रहे थे, वीडियो डिलीट करने के लिए धमकाया जा रहा था – “वीडियो डिलीट कर, वरना मार देंगे”।
18 सितंबर को वे लापता हो गए और 19 सितंबर को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनकी कार अगले ही दिन नदी के पास मिली, और कई दिन बाद भागीरथी नदी के बैराज में उनका शव बरामद हुआ। पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच शुरू की गई, पोस्टमार्टम करवाया गया, और फिर जांच की कार्यवाही ढीली पड़ती गई। हालांकि अंतिम CCTV फुटेज में वे अकेले ही कार चला रहे थे, पर परिवार बार-बार आरोप लगाता रहा कि राजीव को धमकियां दी जा रही थीं, और उनकी मौत साधारण नहीं थी।
मौत के बाद प्रश्नचिह्न: आरोपी, उद्देश्य, और जांच
पुलिस की जांच रिपोर्ट से कई बातें स्पष्ट होती हैं, तो कहीं-कहीं कथित रूप से छुपाने की कोशिश भी नजर आती है। पुलिस का कहना है कि अंतिम फुटेज में वे अकेले थे, किसी दोस्त या जान-पहचान वाले के साथ नहीं थे, घरवालों ने अपहरण की आशंका जताई थी इसलिए पहले गुमशुदगी, फिर अपहरण का केस दर्ज किया गया। हालांकि, किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा, न ही कॉल रिकॉर्डिंग या अन्य सबूत में किसी खास संदिग्ध का नाम सामने आया। परिवार की बार-बार शंका को “अनुमान” मानकर जांच की जा रही है – आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार का बहाना बनाया जा रहा है।
घटनास्थल और शव मिलने की जगह के बीच की दूरी, नदी के प्रवाह, और कार की लोकेशन – यह सब स्थानीय पुलिस द्वारा जारी क्लिच है, जिससे सवाल उठता है कि क्या मामला सुलझाने का असल इरादा है या केवल मीडिया और परिवार को शांत करने की औपचारिकता पूरी की जा रही है।
पत्रकारों की सुरक्षा: भारत की सच्चाई
यह कोई पहली घटना नहीं है जब किसी पत्रकार ने भ्रष्टाचार को उजागर किया और उसकी हत्या हो गई। छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर, रेत माफिया, खनन घोटाले, ज़मीन विवाद – भारत में पत्रकारों पर हमले आम होते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई पत्रकारों की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने सांसद, विधायक, माफिया या व्यवस्था की पोल खोली। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे मामलों को नेशनल न्यूज नहीं बनाया जाता। मीडिया की मुख्यधारा में वे खबरें गुम हो जाती हैं, स्थानीय मीडिया या स्वतंत्र पत्रकार ही शोर मचाते हैं, बड़े चैनल्स, प्रमुख पत्रकार इस पर बहस नहीं करते।
कोई कानून, कोई सुरक्षा तंत्र, कोई बीमा, कोई हेल्थ गारंटी – भारत में छोटे या स्थानीय पत्रकारों के लिए ऐसा कोई आश्वासन नहीं है। वे कभी भी कानून, अपराध, माफिया, नेता, पुलिस या किसी भी सत्ता के खिलाफ रिपोर्टिंग करते वक्त अकेले रह जाते हैं। न उन्हें सरकारी संरक्षण मिलता है, न ही समाज का समर्थन। कानून में पत्रकार सुरक्षा का प्रावधान तो है, पर अमल नाममात्र का है। सच्चाई यह है कि दबंग पत्रकार या बड़े मीडिया संस्थान के रिपोर्टर अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित होते हैं, लेकिन छोटे पत्रकार – जिला, तहसील, कस्बा स्तर – के लिए तो कोई सामाजिक या कानूनी सुरक्षा नहीं है।
राजनीति और पत्रकारिता: सवालों के घेरे में सिस्टम
राजीव प्रताप की हत्या के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने जांच का आश्वासन दिया, परिवार को मुआवजा या नौकरी देने की बात कही – लेकिन अंततः सच्चे पत्रकारों के लिए वातावरण भय मुक्त बनाने की दिशा में कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। जो पत्रकार छोटी जगहों पर, सीमित साधनों में, ईमानदारी से अपने जिले-तहसील-कस्बे की सच्चाई उजागर करते हैं, वे सबसे बड़ा खतरा उठाते हैं। मुख्य मीडिया स्ट्रीम में बड़े पत्रकारों को तवज्जो मिलती है, मोटी तनख्वाह मिलती है, बड़ी सुरक्षा मिलती है – लेकिन छोटे पत्रकारों के लिए मौत बेहद सस्ती है।
कई बार राजनीतिक दबाव, प्रशासन की मिलीभगत, सत्ता के दलाल ऐसे मामलों को रफा-दफा करने में लगे रहते हैं। कई मामलों में परिवार डर की वजह से चुप रह जाता है, गवाह मुकर जाते हैं, और जांच रिपोर्ट को क्लोज कर दिया जाता है। इस बार भी राजीव के परिवार ने जांच की मांग तो की, लेकिन किसी खास व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सके, जिससे पुलिस को प्रकरण रफा-दफा करने की छूट मिली है। सवाल उठता है कि क्या ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्वतंत्र जांच, निष्पक्षता और दोषियों को कड़ी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए।
सोशल मीडिया और जन आंदोलन: सच को आवाज देने की जद्दोजहद
बड़े चैनलों पर बहस न हो, नेशनल न्यूज न बने – तो क्या लेख, रील्स, ट्वीट्स के जरिए आम आदमी सच की लड़ाई लड़ सकता है? ‘न्यूज पिंच’ रिपोर्टर अभिनव पांडे ने कहा कि सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपने-अपने स्तर पर आवाज उठा सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि सभी दर्शक, पाठक, सोशल मीडिया यूजर्स – चाहे वे Instagram, X (Twitter), Facebook, WhatsApp पर हों – इस बारे में लिखें, अभियान चलाएं, पोस्ट करें, ऐसे पत्रकारों को न्याय दिलाने के लिए जनमत बनाए।
अब मीडिया का मतलब केवल न्यूज चैनल या अखबार नहीं रह गया है। आम आदमी वीडियो बनाकर, लिखकर, पोस्ट करके सच समाज तक पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में स्थानीय पत्रकारों की हत्या की खबरें कभी मुख्यधारा के मीडिया में जगह पा सकेंगी? क्या सोशल मीडिया का जन आक्रोश सरकार, पुलिस, प्रशासन को सचमुच न्याय की राह पर डाल सकेगा?
पत्रकारिता का भविष्य: खतरों की छाया में सच की खोज
पत्रकारिता का असल उद्देश्य नागरिकों को सच बताना, सत्ता के दुरुपयोग पर सवाल उठाना, और लोकतंत्र की रक्षा करना है। लेकिन जब सच बोलना मौत का कारण बन जाए, तब यह पेशा सबसे खतरनाक बन जाता है। भारत जैसे देश में, जहां राजनीतिक दल, अपराधी, अधिकारी, माफिया सब मिलकर सच छुपाने का खेल खेलते हैं, वहां स्थानीय पत्रकार सच लिखने से पहले बार-बार सोचता है।
छोटे शहर-कस्बों का सच्चा पत्रकार आज दोराहे पर खड़ा है – एक तरफ सच की चाहत, दूसरी तरफ जान का डर। राजीव प्रताप, मुकेश चंद्राकर जैसे नाम केवल केस स्टडी नहीं हैं, बल्कि वे हमारे समाज की उदास सच्चाई हैं – कि इस देश में सबसे सस्ती चीज पत्रकार की जान है।
पत्रकारिता की राह में बंदूक
आमतौर पर पत्रकार होने का अर्थ मोटी सैलरी, ग्लैमर, पावर और सच्चाई का रक्षक होना समझा जाता है। पर भारत जैसे देश में, खासकर छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में, पत्रकार ब्रेकिंग न्यूज़ से दूर बेखौफ होकर खबर करने का साहस करता है। लेकिन यही साहस उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। अस्पताल की गंदगी, खनन का घोटाला, नेता-अफसरों की मिलीभगत, माफिया का आतंक, दलालों का खेल – इन सबसे सामना करना जिस पत्रकार का रोज का काम है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है खुद को और अपने परिवार को सुरक्षा देना।
पत्रकारिता आज बंदूक की नाली के नीचे है। हर खबर, हर रिपोर्टिंग, हर वीडियो का मतलब है – धमकियां, फोन, पीछा करना, अपहरण, हत्या। कई बार हत्या को हादसा बना कर दिखाया जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देर से जारी किया जाता है, पुलिस जांच को लंबा खींचा जाता है।youtube
पुलिस-प्रशासन: प्रोटोकॉल से आगे सोच कब?
स्थानीय पुलिस और प्रशासन की भूमिका सवालों के कटघरे में है। केस दर्ज करना, गुमशुदगी की तलाश, पोस्टमार्टम, जांच; यह सब मात्र औपचारिकता बन गया है। परिवार की शंका को गंभीरता से न लेना, धमकियों की जांच न करना, गवाहों को सुरक्षा न देना, स्वतंत्र जांच टीम का गठन न करना – यह सब सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। “क्या जांच सही दिशा में बढ़ेगी?”, “क्या आरोपियों को सजा मिलेगी?” – ऐसे सवाल हमेशा अनुत्तरित रहते हैं।
परिवार का दर्द: न्याय या सांत्वना?
एक पत्रकार की मौत उसके परिवार के लिए केवल व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि सामाजिक असुरक्षा और व्यवस्था में विश्वास की हार भी है। पत्नी का दर्द, बच्चों की बेबसी, बूढ़े मां-बाप की चिंता – यह सब हर पत्रकार के परिवार की कहानी बन गई है। मुआवजा, नौकरी, और सांत्वना का वादा बार-बार दोहराया जाता है; लेकिन असली न्याय दूर की कौड़ी। जब तक दोषियों को सजा न मिले, परिवार की पीड़ा खत्म नहीं होती। टाइम पर न्याय मिलने की उम्मीद हर बार टूटती है।
समाज की भूमिका: गतिविधि से आगे
राजीव प्रताप की खबर दिल्ली से दूर थी, उत्तरकाशी के सीमांत जिले की थी। बड़े चैनल्स ने खबर नहीं चलाई, सोशल मीडिया का शोर भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा – तब क्या समाज की ज़िम्मेदारी यही है कि ट्रेंड, पोस्ट, ट्वीट करके पीछे हट जाए? नहीं। ऐसे मामलों में समाज का दबाव, जन आंदोलन, और लोकतंत्र का असली स्वरूप सामने आना चाहिए। जब तक सच्चाई को मुकाम नहीं मिलता, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, जब तक पत्रकारिता भय मुक्त नहीं होती – तब तक समाज को आवाज उठाते रहना चाहिए।
निष्कर्ष: कब तक?
राजीव प्रताप का नाम सूची में एक और नाम बनकर रह गया है। मुकेश चंद्राकर, रवीश कुमार की धमकियों, शशिकांत की हत्या – देश में पत्रकारिता का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सवाल यही है कि कब तक? आखिर कब तक भ्रष्टाचार उजागर करना पत्रकारों के लिए मौत का सामान बना रहेगा?
सरकार से, प्रशासन से, सांसद-विधायकों से, पुलिस से – समाज को जवाब चाहिए। कब तक न्याय को टाला जाएगा, कब तक दोषियों को बचाया जाएगा, कब तक रिपोर्टर की जान सस्ती रहेगी? पत्रकारिता का असल सवाल यही है।
इस देश में पत्रकारों की मौत पर मातम नहीं, व्यवस्था बदलने की ललक होनी चाहिए। उनके हत्यारों को सजा मिले, उनके परिवार सुरक्षित हों, और पत्रकारिता भय मुक्त हो – इस लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी है। आज राजीव प्रताप के लिए आवाज उठाइए, ताकि कल और कोई राजीव प्रताप, कोई मुकेश चंद्राकर मौत के मुंह में न जाए।
अस्वीकरण: उपरोक्त लेख अभिलेखित रिपोर्ट, परिवार के अनुभव, पुलिस के बयान और न्यूज पिंच ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर लिखा गया है। समाज, सरकार और मीडिया के रवैये का संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास है।youtube
आइए, पत्रकारिता के इस दुर्दिन में न्याय की मांग को बुलंद करें।