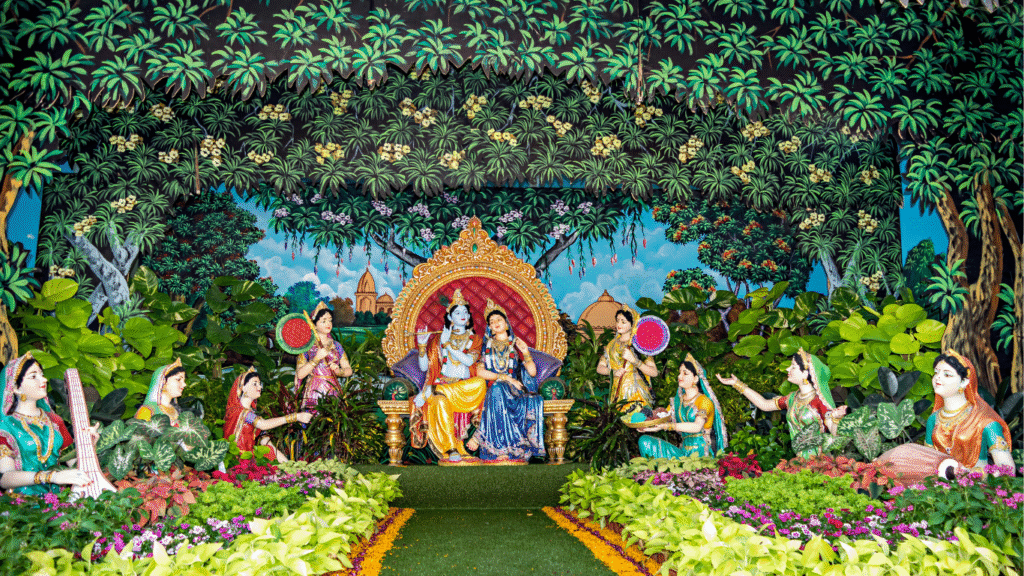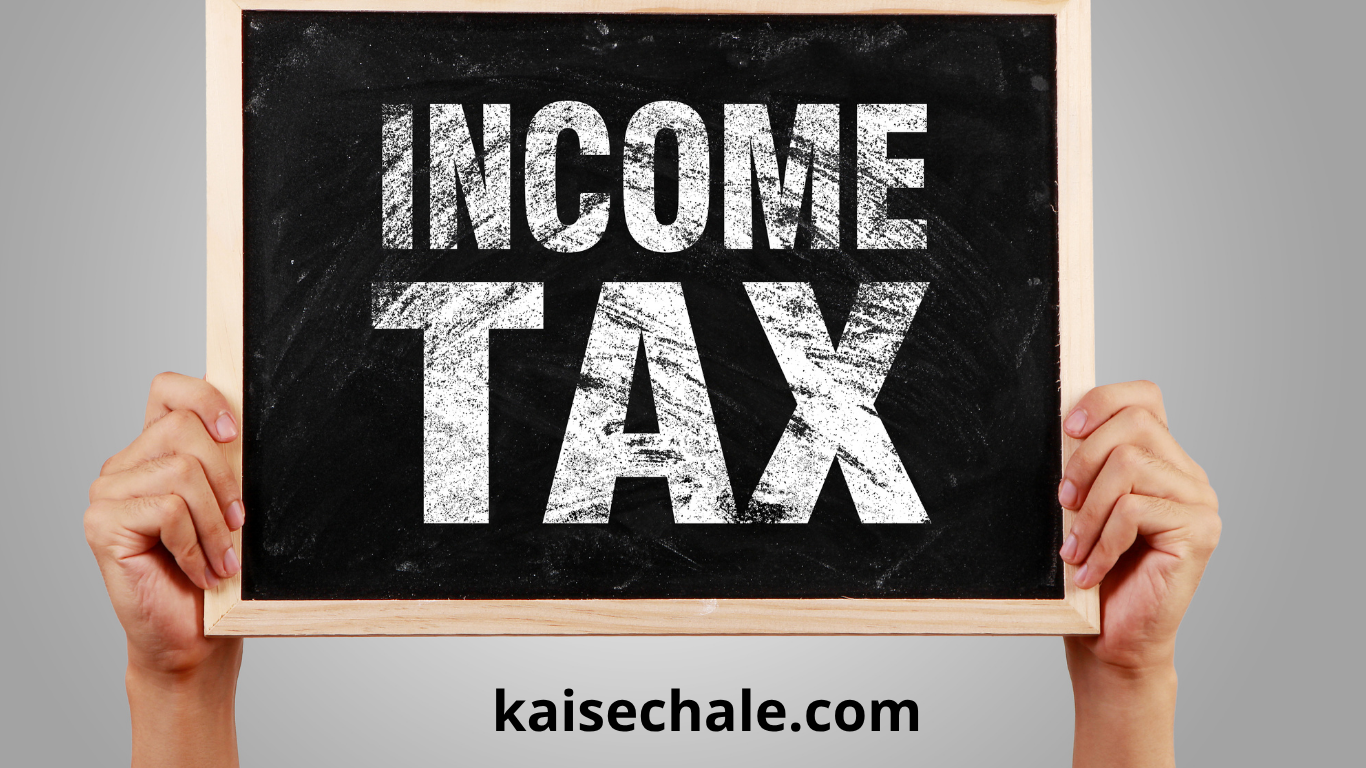इस लेख में बताया गया है कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को संन्यास का मार्ग न अपनाने और अपना धर्म निभाते हुए युद्ध करने के लिए क्यों कहा था। प्रेमानंद महाराज के विचारों के अनुसार, मनुष्य का जीवन अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए मिला है, और संघर्ष एवं कर्म ही व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं। नीचे लेख की मुख्य बातें 3000 शब्दों के विस्तार में हिंदी में दी जा रही हैं, जिसमें हर विचार को विस्तार से समझाया गया है।
अर्जुन का संन्यास लेने का विचार
महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन धर्म-संकट में पड़ गए थे। वे सोचने लगे थे कि क्या युद्ध करना सही है, या वे संन्यास लें और संसार के मोह-माया से दूर हो जाएं। इस स्थिति में श्रीकृष्ण ने उन्हें योग, कर्म, और धर्म का महत्व समझाया।
श्रीकृष्ण की शिक्षा: कर्म और धर्म
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी थी कि सिर्फ संन्यास लेने मात्र से व्यक्ति को अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती। इंसान के पास जो कर्तव्य है, वह उसे जरूर निभाना चाहिए। यहां ‘करो या मरो’ की भावना नहीं, बल्कि ‘स्मरण करते हुए कर्म करना’ की शिक्षा थी। भगवान ने कहा—
“सर्वदा सर्वकाले निर्युद्ध्य च,”
अर्थात हमेशा भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का संपादन करो।
स्वधर्म और परधर्म
श्रीमद्भगवद्गीता में लिखा है—
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः”
यानि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म अपनाना व्यक्ति के लिए भयावह है। अर्जुन क्षत्रिय थे, और उनका धर्म था युद्ध में भाग लेना। उनके लिए संन्यास उस समय उचित नहीं था; उन्हें पहले अपना धर्म और कर्तव्य निभाना आवश्यक था।
जीवन का संघर्ष
परम पूज्य प्रेमानन्द महाराज कहते हैं कि जीवन का असली अर्थ संघर्ष और मेहनत में है। अगर इंसान संघर्ष करना बंद कर दे, तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। संघर्ष ही इंसान को मजबूत और समझदार बनाता है। अर्जुन के जीवन का संघर्ष ही उन्हें महान योद्धा बनाता है; इसी तरह हर व्यक्ति का जीवन संघर्षों का संग्राम है।
कर्म ही पूजा है
भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कर्म करते हुए भगवान के स्मरण की सलाह दी। इसका मतलब है—
कोई व्यक्ति शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील है या किसान है—हर व्यक्ति को अपने कार्य को भगवान का नाम लेते हुए करना चाहिए। यही उसकी पूजा है, और उसे उसी में सिद्धि प्राप्त होती है।
संत रविदास का उदाहरण
परम पूज्य प्रेमानंद महाराज ने संत रविदास जी का उदाहरण देते हुए बताया कि वे गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, लेकिन उन्होंने अपने कर्म को ही पूजा माना। एक बार संत रविदास ने पंडित जी से कहा, “गंगा स्नान के समय मेरे लिए दो केले गंगा को अर्पित करना।” पंडित जी ने केले गंगा में अर्पित किए, तो गंगा जी के जल से हाथ निकला, जिसने केले स्वीकार किए और बदले में स्वर्ण कंगन दिये। इस चमत्कार से स्पष्ट हुआ-
“मन चंगा तो कठौती में गंगा”
यानि मन शुद्ध है तो वही स्थान तीर्थ बन जाता है। कर्म को पूजा मानकर, संत रविदास सिद्धि को प्राप्त हुए।aajtak
अर्जुन के लिए युद्ध धर्म क्यों था?
परम पूज्य प्रेमानंद महाराज विस्तार से बताते हैं—
जैसे अर्जुन के लिए युद्ध धर्म था, वैसे ही हर व्यक्ति के लिए उसका कर्म धर्म है। भगवान ने जो काम आपको दिया है, उसे धर्मपूर्वक, सत्यपूर्वक और भगवान के स्मरण के साथ करने से ही जीवन सफल बनता है। जब तक मनुष्य का कर्तव्य बाकी है, कर्म करना ही श्रेष्ठ है।
भगवान केवल नाम के स्मरण और कर्म की ईमानदारी से प्रसन्न होते हैं। अगर हम अपने कर्म में बेईमानी छोड़ दें और भगवान का नाम लेते हुए अपना कार्य करें, तभी जीवन में सिद्धि मिलती है। कर्तव्य के प्रति समर्पण और निष्काम भाव ही भगवत् प्राप्ति का मार्ग है।
अर्जुन, संन्यास और युद्ध
अर्जुन का संन्यास लेने का विचार क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध था। श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया—
संन्यास बाद में लिया जा सकता है, पर पहले अपने धर्म और कर्तव्य का पालन आवश्यक है। युद्ध करते समय भगवान का स्मरण ही उच्चतम पूजा है।
जीवन के संघर्ष में भगवत-प्राप्ति
परम पूज्य प्रेमानंद महाराज की शिक्षा है—
हर व्यक्ति को जीवन के संघर्ष और चुनौती का सामना करते हुए भगवान के स्मरण के साथ अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। यही जीवन का जादू है, जब मनुष्य अपनी मेहनत, संघर्ष और कर्म को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने लगता है।
निष्कर्ष: कर्म ही धर्म है
अर्जुन के प्रसंग में श्रीकृष्ण का संदेश है कि कर्म ही धर्म है। भगवान के दिए कार्य को श्रद्धा, सत्य और स्मरण के साथ करते रहना, यही जीवन की संतुष्टि और अध्यात्म की प्राप्ति का मार्ग है। जब तक जिम्मेदारियां बाकी हैं, उन्हें निभाना ही सर्वोच्च धर्म है। संन्यास बाद में लिया जा सकता है, पर पहले अपने कर्तव्य का निवर्हन ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।
यह लेख मुख्य रूप से परम पूज्य प्रेमानंद महाराज के उपदेश, श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोकों और संत रविदास के उदाहरणों पर आधारित है। इसमें कोई अलग स्रोत सन्दर्भित नहीं है, लेख के विचार प्रेमानंद महाराज के ही हैं और संदर्भ के तौर पर श्रीमद्भगवद्गीता का ही उद्धरण आता है।